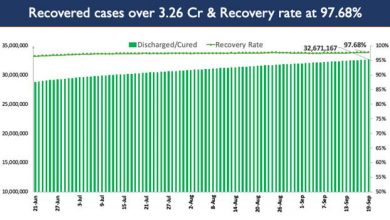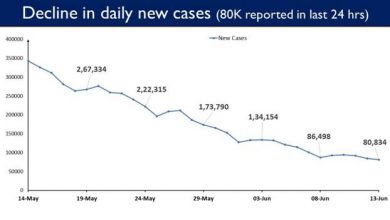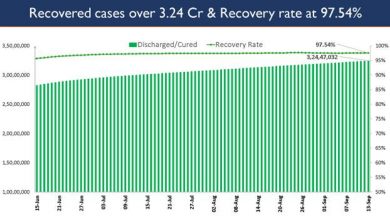चार बुखार से बचाएगी एक सावधानी एक मच्छरदानी डा. उपेन्द्रमणि त्रिपाठी

मच्छरों से होने वाले बुखार- डेंगू, चिकनगुनिया, जापानीज इंसेफेलाइटिस और मलेरिया
सरकारी जागरूकता के प्रयासों के बावजूद स्वच्छता के प्रति हमारी लापरवाही जीवन के लिए संकट की स्थिति पैदा कर सकती है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है पिछले कुछ वर्षों में मच्छरों से फैलने वाले भयंकर महामारी का रूप लिए बुखार के कई प्रकार। मानवता पर एक मच्छर , ड्रोन हेलीकाप्टर की तरह बारूद (रोगकारकों) को सीधे अपने दुश्मन (मनुष्य के रक्त) पर लांच कर देता है।
ज्यादा खतरा कब –
डॉ उपेन्द्र मणि त्रिपाठी के अनुसार जुलाई-अगस्त से अक्टूबर तक बरसात के समय व उसके बाद हमारे घरों में पुराने गड्ढे, नाली, कूलर, टँकी, या अन्य पड़े सामानों, घर के आस पास एकत्र पानी व गंदगी मच्छरों के प्रजनन व पनपने की सबसे मुफीद जगह होती हैं।
कैसे फैलता है रोग –
डॉ उपेन्द्र मणि त्रिपाठी ने बताया मनुष्यो को मादा ही काटती हैं किन्तु रोग केवल संक्रमित मच्छर से ही फैलता है। इनकी आंत में रोगाणुओं ,जीवाणुओ, विषाणुओं ,परजीवियों को पनपने की जगह मिल जाती है और हमारा रक्त चूसते समय उसकी लार के साथ यह रोगकारक मनुष्य के रक्त में मिल कर पहले अपने लिए उचित जगह (प्रमुख रूप से लिवर कोशिकाओं ) बनाते हैं, फिर अपनी संख्या बढ़ाते हैं तब कई दिनों बाद रोग के लक्षण पैदा करते है। काटे जाने से लेकर रोग लक्षण दिखने के बीच इस समय को इन्क्यूबेशन पीरियड कहा जाता है।
कब दिखाई पड़ते हैं लक्षण –
संक्रमित मच्छर के काटने के तुरन्त बाद रोग के लक्षण नहीं मिलते बल्कि इसके कुछ दिनों बाद पैदा होते हैं
डेंगू बुखार- 3 -5 दिन
चिकनगुनिया- 2 -7 दिन
मलेरिया – 7 से 10 दिन बाद लक्षण प्रकट हो सकते हैं।
किस मच्छर से कौन सा खतरा-
भारत में प्रमुख रूप से
एडीज-डेंगू, चिकनगुनिया,
एनफेलिस-मलेरिया
क्यूलेक्स – जापानीज़ इंसेफ्लाईटिस
यह जानना भी जरूरी है कि
डेंगू ,चिकनगुनिया और जे ई विषाणु से होने वाले रोग हैं जबकि मलेरिया प्रोटोजोआ परजीवी प्लासमोडियम की पञ्च प्रजातियों में से किसी एक के संक्रमण से होता है।
कैसे पहचानें रोग
डॉ उपेन्द्र मणि त्रिपाठी ने कहा रोग से ग्रसित व्यक्ति में शुरुआत में लगभग एक समान लक्षण प्रकट होने से बुखार के प्रकार को समझ पाना आमजन के लिए आसान नही होता। व्यक्ति को सामान्यतः तेज बुखार (102-105 डिग्री फारेनहाइट तक), सिरदर्द,पूरे शरीर में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी, भूख कम लगना, कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ऐसे समय बिना चिकित्सक को दिखाए केवल बुखार उतरने की दवा खाने से उचित नही होगा।
कैसे पहचानें अलग अलग बुखार को-
डॉ उपेन्द्र मणि त्रिपाठी ने बताया मलेरिया को जूड़ी ताप बुखार भी कहते है । यह पारी देकर आता है। रोगी को पहले तेज ठण्डी लगती है फिर तेज बुखार चढ़ता है इसके बाद तेज पसीना होता है। कुछ मरीजों में बुखार के समय प्यास का लक्षण भी पाया जाता है। हमारे देश में प्लाज्मोडियम वाईवेक्स और फाल्सीपैरम प्रजाति के परजीवी से होता है। फैलसिपैरम छः महीने में पुनः हो सकने की सम्भावना के साथ ज्यादा खतरनाक होता है। इसके परजीवी लिवर व लालरक्तकोशिकाओं पर आश्रित होते हैं इसलिए पीलिया और अनीमिया की सम्भावना भी होती है।
इसीप्रकार चिकनगुनिया में भी ठण्डी के साथ तेज बुखार आता है, इसमे खास लक्षण होता है कि व्यक्ति को मांसपेशियों के साथ जोड़ों में तेज दर्द, प्रकाश से भय, शरीर पर चकत्ते नजर आने के साथ जोड़ो में सूजन व विकृति उत्पन्न होने की भी सम्भावना होती है।
जबकि डेंगू वायरस से होने वाले बुखार में तेज बुखार के साथ शरीर में हड्डियों के टूटने जैसा दर्द होता है, इसीलिए इसे “ब्रेक बोन फीवर” भी कहते हैं।यह वायरस चार प्रकार का होता है। इसका मच्छर एडीज काली सफेद धारी वाला होता है जिसे बाघ मच्छर भी कहते हैं यह दिन में काटता है। लक्षणों के आधार डेंगू तीन प्रकार से प्रकट हो सकता है, पहला साधारण प्रकार जो स्वयं ठीक हो सकता है, किन्तु दूसरा और तीसरे प्रकार का डेंगू जिसे डेंगू हैमरेजिक फीवर व डेंगू शाक सिंड्रोम कहते है यदि समय पर उपचार न मिले तो प्राणघातक सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि इसमे रक्त कण टूटने से प्लेटलेट्स की संख्या में गिरावट आने लगती है जिससे रक्त स्राव हो सकता है। त्वचा के नीचे लाल चकत्ते नजर आने लगते हैं, आँखों में दर्द विशेष लक्षण हैं।
इसी प्रकार तराई इलाकों में जहां धान की खेती अधिक होती है वहां पनपने वाले मच्छर क्यूलेक्स विश्नोई के जरिये जैपनीज इंसेफ्लाईटिस का विषाणु बहुधा 5-15 वर्ष के बच्चों को संक्रमित कर सकता है। इससे प्रभावित रोगी बुखार के बताये गए लक्षणों के साथ गर्दन में ऐंठन व अकड़न का विशेष लक्षण पाया जाता है।
क्या हैं तेज बुखार में अंतर के विशिष्ट लक्षण-
1. मलेरिया- पारी देकर तेज बुखार,
2. डेंगू – हड्डी टूटने जैसा दर्द और शरीर पर चकत्ते।
3. चिकनगुनिया- जोड़ों में सूजन दर्द और विकृति।
4.जापानीज़ इंसेफ्लाईटिस – गर्दन में अकड़न ।
रक्त जाँच से करें रोग की पुष्टि-
जुलाई से सितम्बर के मध्य होने वाले बुखार के प्रकार की जाँच के लिए चिकित्सक के परामर्श के अनुसार रक्त परीक्षण, आरटीपीसीआर या रिवर्स ट्रांस्क्रिप्टेज पालीमेरेज चेन रिएक्शन,अथवा एलिसा रक्त जांच से रोग की पुष्टि की जाती है।
क्या बरतें सावधानी-
अपने घर व आस पास स्वच्छता का विशेष ध्यान दें, नमी गन्दगी व पानी न एकत्र होने दें, नालियों में कीटनाशक या मिटटी के तेल का छिड़काव कराएं। रात में मच्छरदानी में ही सोएं व दिन में व शाम के समय मच्छरों से बचने के लिए पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, क्रीम ,जेल या नीम तेल का प्रयोग कर सकते है। पौष्टिक आहार लें।
मच्छरों से सुरक्षा का सबसे कारगर उपाय है मच्छरदानी, सोते समय अवश्य प्रयोग करना चाहिए।
क्या करें घरेलू उपाय-
अजवायन किशमिश तुलसी और नीम की पत्तियो को उबाल कर पेय को दिन में 3-4 बार ले सकते हैं।
पपीते की पत्ती का जूस प्लेटलेट्स की संख्या को नियंत्रित करने के लिए जाना जाता है इसका भी सेवन कर सकते हैं। स्नान करते समय गर्म पानी में नीम की पत्ती व सेंधा नमक डालकर इसे पानी में मिलाकर नहाएं।
होम्योपैथी में क्या है सम्भव उपचार-
डॉ उपेन्द्र मणि त्रिपाठी के अनुसार उपचार की दृष्टि से विषाणुजनित रोगों में होम्योपैथी का अद्वितीय स्थान है किन्तु औषधियों का चयन व्यक्ति विशेष के लक्षणों के मिलान के आधार पर ही सम्भव है इसलिए बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा लेना उचित नही कहा जा सकता।लक्षणों की गम्भीरता के अनुसार चिकित्सालय में चिकित्सक की नियमित देखरेख में ही उपचार कराना उचित है। यूँ तो डेंगू , चिकनगुनिया, मलेरिया, दिमागी बुखार के लिए प्रतिरोधक दवाये उपलब्ध नही हैं किन्तु होम्योपैथी में जीनस एपिडेमिकस ही प्रतिरोधक के तरह प्रयोग की जा सकती है। 2010 में अमेरिकन जर्नल ऑफ इंफेकशियस डीसीसेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट में जेई के वायरस पर होमयिपैथी की औषधि की प्रभाविता पाई गई है।
अध्ययनों के आधार पर डेंगू एवं चिकनगुनिया , जेई के लक्षणों व युपेटोरियम पर्फ , ब्रायोनिया, ऑसीमम ,बेलाडोना आदि औषधियों के लक्षणों में समानता मिलती है इसलिए इन्हें होम्योपैथिक उपचार व प्रतिरोधक की तरह भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कैरिका पपाया ,आर्स, जेल्स, ब्रायो, बेलाडोना,क्यूप्रम मेट, नैट म्यूर, बेल, क्रोटेलस, इपेकाक, चायना, चिनियमसल्फ, निकटेन्थस, टीनोस्पोरा कार्डीफोलिया आदि दवाएं उपचार में बेहतर हो सकती हैं।